Новости



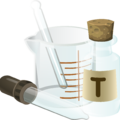




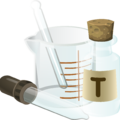


Формировать умение сравнивать равные (неравны группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов предметов), пользуясь приёмами последовательного приложения предметов одной группы к предметам другой

Сформировать у детей понимание об изменении и эволюции стилей, материалов и функций одежды и обуви в прошлом и настоящем, развивая их восприятие и понимание исторического контекста моды для расширения культурных знаний и навыков анализа.

Развитие навыков вопросительной речи у детей 5-6 лет через игры и интерактивную деятельность.

Квест разработан для детей старшего дошкольного возраста. Готовый квест для проведения в группе или на территории прогулочных площадок детского сада.

Квест подойдёт для детей младшего дошкольного возраста. Готовый квест для проведения в группе или на территории детского сада

Квест рассчитан на младшую группу детского сада. Готовый сценарий увлекательного и позновательного квеста для детей с готовыми заданиями.
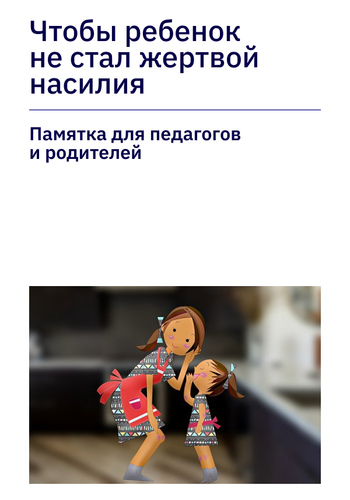
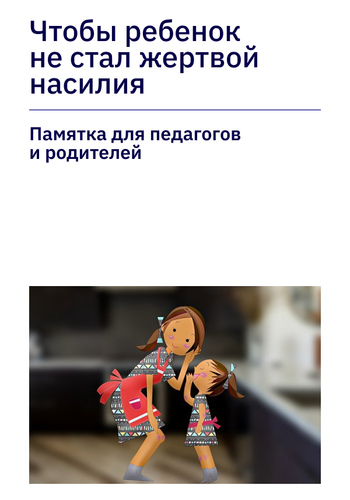
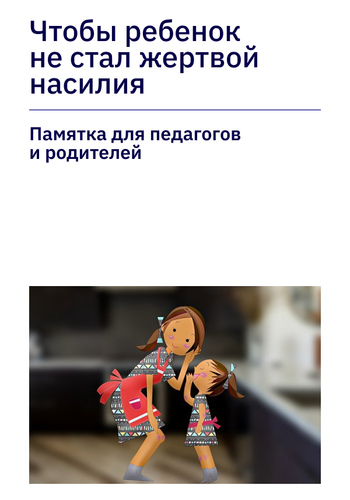
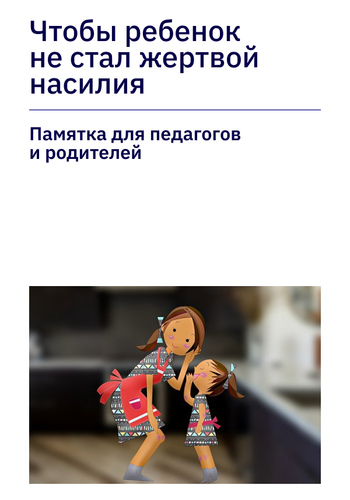
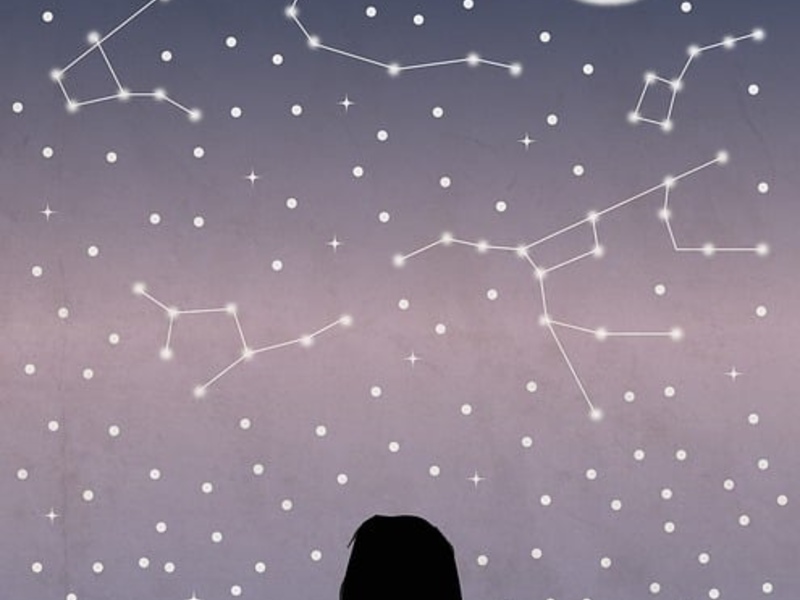
Данный проект поможет детям научиться добывать информацию из разных источников, систематизировать полученные знания, применять их в различных видах детской деятельности

Доброта и милосердие – это высочайшие нравственные ценности, вершина человеческого духа. В них проявляются гармония чувств, мыслей, поступков; готовность помочь кому-нибудь или простить кого-либо из сострадания
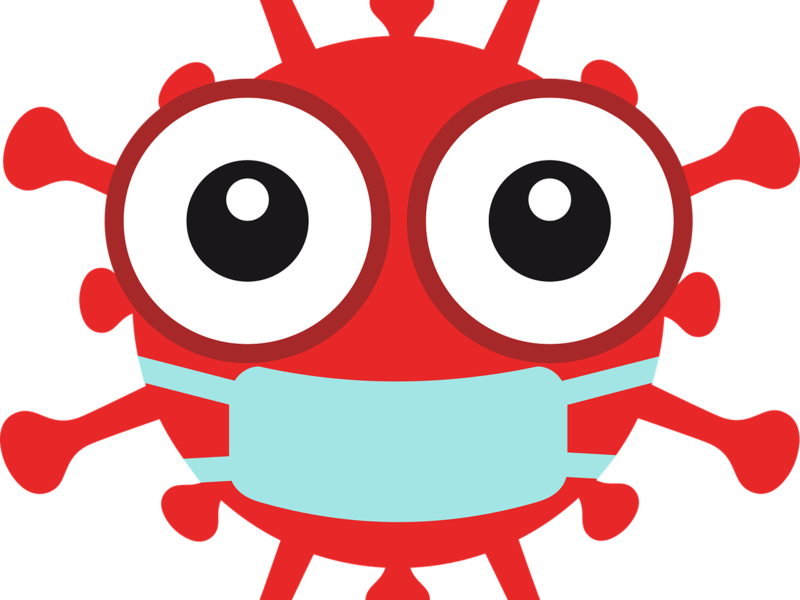
Опытно – экспериментальный проект. На идею и реализацию проекта подтолкнула эпидемия и детские ручки, которые постоянно трогают лицо и рот.

Лэпбук на тему "Осень" - интерактивное развивающее пособие для детей дошкольного возраста.

Лэпбук на тему "Насекомые" - интерактивное развивающее пособие для детей дошкольного возраста.

Лэпбук на тему "Весна" - интерактивное развивающее пособие для детей дошкольного возраста.


Без внимания ребенок не может самостоятельно выполнить задание или поручение взрослого.

В свободные минуты бодрствования займитесь с крохой мимико-артикуляторной гимнастикой.

Упражнения, которые помогут вашему малышу научиться правильно произносить звуки [С] и [З]